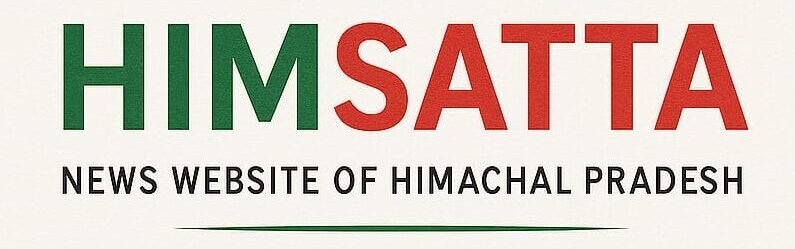राजन कुमार शर्मा: ऊना जिला हिमाचल प्रदेश का एक सुंदर और कृषि प्रधान क्षेत्र है, लेकिन बरसात के मौसम में यहाँ जलभराव की समस्या गंभीर रूप से देखी जाती है। भारी वर्षा के कारण नालों और नदियों में पानी का स्तर बढ़ जाता है, जिससे सड़कों, खेतों और घरों में जलभराव हो जाता है। यह समस्या न केवल लोगों की दैनिक जीवनशैली को प्रभावित करती है, बल्कि स्वास्थ्य, यातायात और कृषि को भी नुकसान पहुंचाती है।जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश अपनी भौगोलिक स्थिति और निर्माण ढांचे के कारण हर वर्ष बरसात के मौसम में जलभराव (Water Logging) की समस्या से जूझता है। जब भारी वर्षा होती है तो शहर एवं ग्रामीण इलाकों में उचित जल निकासी तंत्र (Drainage System) के अभाव में सड़कों, गलियों और घरों के आसपास पानी भर जाता है। यह स्थिति आमतौर पर एक-दो सप्ताह तक ही रहती है, परंतु इन दिनों में नागरिकों को भारी असुविधा, यातायात अवरोध और स्वास्थ्य संबंधी खतरे झेलने पड़ते हैं।
समस्या की जड़:
1. भूगोल एवं स्थलाकृति (Geography & Topography) – ऊना का क्षेत्र अपेक्षाकृत समतल है, जिससे वर्षा का पानी प्राकृतिक रूप से शीघ्र नहीं निकल पाता।
2. अपर्याप्त जल निकासी प्रणाली – वर्तमान में नालियों एवं ड्रेनेज का जाल बरसाती पानी के दबाव को झेलने योग्य नहीं है।
3. अनियोजित निर्माण – आवासीय और व्यावसायिक भवनों का निर्माण बरसात की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर नहीं किया गया है। 4. जनता में जागरूकता की कमी* राष्ट्रीय राजमार्गों, सड़कों व आवासीय कॉलोनियों तथा रिहायशी शहरी क्षेत्रों में बनी हुई जल निकासी/नालियों में कुछ लोगों द्वारा घरेलू कचरा व गंदगी डालने से अवरोध उत्पन्न होता है। जो कि बाद में जल भराव जैसी समस्याओं को उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार होता है
5.*सड़क और यातायात बाधित होना: जलभराव के कारण सड़कें पानी में डूब जाती हैं, जिससे आवागमन कठिन हो जाता है।
6.*फसलों को नुकसान: खेतों में पानी जमा होने से फसलों की पैदावार घटती है।
7. स्वास्थ्य समस्याएं:* जलभराव के कारण मच्छरों का प्रकोप बढ़ता है, जिससे मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ जाता है।
8. सार्वजनिक असुविधा:* जलभराव के कारण स्कूल, अस्पताल और अन्य आवश्यक सेवाओं तक पहुँच प्रभावित होती है।
समाधान की दिशा:
जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान तभी संभव है जब प्रशासन, स्थानीय जनता और विभिन्न संगठनों द्वारा मिलकर काम किया जाए। हम सभी को यह स्वीकार करना होगा कि यह सिर्फ बरसात के दिनों की समस्या नहीं, बल्कि हर वर्ष दोहराया जाने वाला संकट है। इसका समाधान केवल प्रशासन पर छोड़ना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि समाज, पंचायतें, नगर निकाय, तकनीकी विशेषज्ञ और स्वयंसेवी संस्थाओं को मिलकर काम करना होगा।
1. स्थायी जल निकासी प्रणाली का निर्माण – योजनाबद्ध ढंग से मजबूत नालियों एवं स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज की व्यवस्था करना आवश्यक है।
2. सामुदायिक भागीदारी – मोहल्ला स्तर पर जल निकासी व्यवस्था की नियमित सफाई एवं रखरखाव सुनिश्चित करना।
3. भविष्य के निर्माण में सावधानी – भवन निर्माण के समय वर्षा जल निकासी का ध्यान रखना, ताकि नई कॉलोनियां समस्या को और न बढ़ाएँ।
4. तकनीकी अध्ययन – विशेषज्ञों द्वारा ऊना की स्थलाकृति और वर्षा पैटर्न का वैज्ञानिक अध्ययन कर दीर्घकालिक योजना बनाना व जल निकासी 5. व्यवस्था का सुधार: नालों और नदियों की नियमित सफाई और नदियों के मार्ग का पुनः निर्धारण किया जाए ताकि पानी का प्रवाह सुचारू हो सके।
6. स्थानीय स्तर पर जल प्रबंधन: गाँवों और मोहल्लों में जल संचयन एवं निकासी के लिए सामूहिक प्रयास किए जाएँ।
7. जन जागरूकता अभियान: जनता को जलभराव की समस्या, उसके कारणों और समाधान के उपायों के प्रति जागरूक किया जाए।
8. वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण: जलभराव कम करने के लिए पेड़ लगाने और मिट्टी के कटाव को रोकने के उपाय अपनाए जाएं।
9. आपदा प्रबंधन की तैयारी: बरसात के मौसम में आपातकालीन सेवाओं का बेहतर प्रबंध हो और लोग सतर्क रहें।
हमारी जिम्मेदारी:
जिला इंटर एजेंसी ग्रुप (DIAG), व जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ऊना के सहयोग से इस जटिल समस्या के समाधान की दिशा में गंभीरता से कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ऊना का मानना है कि यदि अभी से योजनाबद्ध ढंग से कदम उठाए जाएँ, तो अगली बरसात से पहले इस चुनौती पर काफी हद तक काबू पाया जा सकता है। बरसात का मौसम हमारे लिए प्राकृतिक आशीर्वाद है, परंतु यदि हम समय रहते तैयारी न करें तो यही वरदान अभिशाप बन सकता है। इसलिए अब समय आ गया है कि हम सब मिलकर ऊना को जलभराव की समस्या से मुक्त करने के लिए ठोस और स्थायी कदम उठाएँ।
ऊना में जलभराव की समस्या एक जटिल लेकिन सामूहिक प्रयास से सुलझाई जा सकने वाली चुनौती है। यदि प्रशासन, समाज और नागरिक एक साथ मिलकर उचित योजनाओं को अमल में लाएं, तो जलभराव से उत्पन्न असुविधाओं को कम किया जा सकता है और प्राकृतिक आपदाओं का सामना बेहतर ढंग से किया जा सकता है। सामूहिक भागीदारी ही इस समस्या का स्थायी समाधान है।